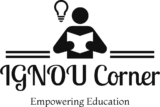परिचय
भगवद्गीता में कर्मसंन्यास का विचार गूढ़ और गहन रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह केवल बाहरी कर्मों के त्याग की बात नहीं करता, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर कर्म से जुड़े अहंकार, इच्छा और फल की अपेक्षा के त्याग की बात करता है। गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सच्चा संन्यास कर्मों का परित्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है।
कर्मसंन्यास का अर्थ
‘कर्म’ का अर्थ है – कार्य, और ‘संन्यास’ का अर्थ है – त्याग। अतः ‘कर्मसंन्यास’ का सीधा अर्थ है – कर्मों का त्याग। परंतु गीता में इसका अर्थ है – फल की भावना और मोह से रहित होकर कर्म करना, और अंततः उस अवस्था तक पहुँचना जब सभी कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं।
श्रीकृष्ण का दृष्टिकोण
अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था और इसे संन्यास समझ रहा था, तब श्रीकृष्ण ने उसे स्पष्ट किया कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म में रहते हुए फल की अपेक्षा का त्याग श्रेष्ठ है। यही गीता में ‘कर्मसंन्यास का भाव’ है।
कर्मसंन्यास के मुख्य तत्व
- निष्काम भाव: फल की इच्छा के बिना कार्य करना।
- अहंकार रहित सेवा: ‘मैं कर रहा हूँ’ का भाव न हो।
- ईश्वर अर्पण भाव: हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर देना।
- आसक्ति का त्याग: कर्मों से मोह न होना।
गीता में उद्धृत श्लोक
“त्याज्यं दोषवत कर्म कर्तव्यं इति मे मतिः”
– गीता अध्याय 18, श्लोक 9
अर्थ: त्याग करने योग्य कर्म वे नहीं हैं जिन्हें दोषपूर्ण मानकर त्यागा जाए, बल्कि वे हैं जिन्हें कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किया जाए।
कर्मयोग और कर्मसंन्यास का संबंध
श्रीकृष्ण कर्मयोग को कर्मसंन्यास से श्रेष्ठ मानते हैं। उनका कहना है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन मन को ईश्वर में लगाकर और फल की चिंता किए बिना।
व्यावहारिक दृष्टिकोण
- एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए कर्तव्य करता है, परंतु मोह में नहीं बंधता – वह भी कर्मसंन्यासी हो सकता है।
- कर्मों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें योग की भावना से करना ही गीता की सच्ची शिक्षा है।
कर्मसंन्यास की परिणति
- मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन।
- मुक्ति की प्राप्ति – क्योंकि संन्यासी कर्म के बंधन से मुक्त होता है।
- समत्व – सभी स्थितियों में समान भाव।
निष्कर्ष
गीता में कर्मसंन्यास का भाव कर्मों को त्यागना नहीं, बल्कि उनके प्रति मोह और फल की इच्छा का त्याग करना है। यह शिक्षाएँ आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, जहाँ व्यक्ति तनाव, अपेक्षा और परिणाम की चिंता में उलझा रहता है। यदि हम कर्मसंन्यास के इस भाव को आत्मसात करें, तो न केवल आध्यात्मिक प्रगति होगी, बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन भी बना रहेगा।