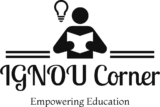परिचय
भगवद्गीता में ध्यानयोग एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य आत्म-शुद्धि, आत्मज्ञान और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति कर सकता है। यह मार्ग मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में साधक को अग्रसर करता है। ध्यानयोग विशेष रूप से गीता के छठे अध्याय में विस्तार से वर्णित है।
ध्यानयोग की परिभाषा
‘ध्यान’ का अर्थ है – मन का एकाग्र होकर किसी एक लक्ष्य या विषय पर स्थिर होना। ‘योग’ का अर्थ है – जोड़ना। इस प्रकार ध्यानयोग वह साधना है जिसमें मन को ईश्वर में स्थिर कर दिया जाता है।
गीता में ध्यानयोग का वर्णन
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यानयोग का अभ्यास करने वाला साधक एकांत स्थान पर, एक सरल आसन पर बैठकर अपने मन को संयमित करता है और निरंतर अभ्यास के द्वारा उसे ईश्वर में स्थिर करता है।
“तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतः चित्तेन्द्रिय क्रियाः।
उपास्यते योगं योगी, मुनिः शान्ति निगच्छति॥”
ध्यानयोग की प्रक्रिया
- एकांत और शांत स्थान का चयन
- सिद्धासन या सुखासन में बैठना
- शरीर, मन और इंद्रियों का संयम
- मन को केवल ईश्वर या आत्मा पर केंद्रित करना
- निरंतर अभ्यास (अभ्यासेन तु कौन्तेय…)
ध्यानयोग के लाभ
- मन की शांति और आत्मिक संतुलन
- इच्छाओं और विकारों पर नियंत्रण
- आध्यात्मिक जागरण और आत्मानुभूति
- मोक्ष की प्राप्ति – जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति
ध्यानयोगी के गुण
- सहनशीलता, नम्रता और संयम
- सभी में परमात्मा को देखना
- सुख-दुख में समान भाव
- निंदा-प्रशंसा में समता
ध्यानयोग और अन्य योगों का संबंध
ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग से जुड़ा हुआ है। गीता कहती है कि ध्यानयोगी वही सच्चा योगी है जो ज्ञान में स्थिर हो, कर्म में समर्पित हो और भक्ति में लीन हो।
आधुनिक युग में ध्यानयोग की प्रासंगिकता
आज के तनावपूर्ण जीवन में ध्यानयोग मानसिक तनाव, चिंता और विक्षेप को दूर करने का एक प्रभावी उपाय है। यह केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि ध्यान शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है।
निष्कर्ष
गीता के अनुसार ध्यानयोग एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ती है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह साधना न केवल मोक्ष का मार्ग है, बल्कि जीवन को शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण बनाने की प्रक्रिया भी है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए।