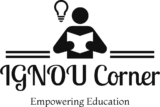परिचय
भगवद्गीता में न केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा की गई है, बल्कि कुछ विशेष शब्दों और अवधारणाओं का उल्लेख भी मिलता है। इनमें ‘योगिनी विद्या’ और ‘गीतामृत’ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों तत्व गीता के सार को समझने में हमारी सहायता करते हैं।
योगिनी विद्या का अर्थ
‘योगिनी विद्या’ का शाब्दिक अर्थ है – वह विद्या जो योग से संबंधित हो। गीता में ‘योग’ का अर्थ है – आत्मा और परमात्मा का मिलन। अतः योगिनी विद्या वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो व्यक्ति को आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर-प्राप्ति की ओर ले जाता है।
योगिनी विद्या के तत्व
- आत्म-नियंत्रण: इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना।
- ध्यान: एकाग्रता द्वारा ईश्वर में मन को लगाना।
- निष्काम कर्म: फल की इच्छा के बिना कार्य करना।
- समत्व योग: सुख-दुख, जय-पराजय में सम रहना।
योगिनी विद्या का उद्देश्य
इस विद्या का मुख्य उद्देश्य है – व्यक्ति को आत्मा की पहचान कराकर ईश्वर से जोड़ना और जीवन को धर्म, शांति व सेवा से भर देना।
गीतामृत का अर्थ
‘गीतामृत’ का अर्थ है – गीता का अमृत स्वरूप, अर्थात् गीता का वह सार जो मनुष्य के जीवन को मधुर, शांतिपूर्ण और दिव्य बना देता है।
गीतामृत के मुख्य बिंदु
- कर्म का संदेश: “कर्मण्येवाधिकारस्ते” – अपने कर्तव्य का पालन करो।
- भक्ति का महत्व: प्रेमपूर्वक भगवान का स्मरण करो।
- ज्ञान का प्रकाश: आत्मा को जानो, अज्ञान का त्याग करो।
- समत्व का भाव: राग-द्वेष से रहित होकर जीवन जियो।
गीतामृत क्यों कहा गया?
गीता के उपदेशों को ‘अमृत’ इसलिए कहा गया है क्योंकि वे नाशवान संसार में भी अमरता का अनुभव कराते हैं। वे केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि आचरण के मार्गदर्शक हैं।
आज के युग में प्रासंगिकता
- जहाँ व्यक्ति तनाव, लालच और भ्रम से ग्रस्त है, वहाँ योगिनी विद्या उसे मन की शांति और आत्मबल देती है।
- गीतामृत से व्यक्ति को जीने की दिशा मिलती है – प्रेम, सेवा और समर्पण के साथ।
निष्कर्ष
योगिनी विद्या और गीतामृत – दोनों ही गीता के अमूल्य उपहार हैं। ये मनुष्य को केवल अध्यात्म की ओर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उच्च आदर्शों की प्रेरणा देते हैं। जो इनका अध्ययन और आचरण करता है, उसका जीवन सफल, शांतिपूर्ण और दिव्य बनता है।