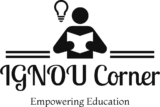परिचय
भगवद्गीता में अप्रकट (अव्यक्त) और प्रकृति (प्रकृत) की अवधारणाओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह दोनों ही तत्व सृष्टि की संरचना, आत्मा की स्थिति और ईश्वर की भूमिका को समझने में सहायक हैं। इस लेख में हम गीता के अनुसार ‘अप्रकट’ और ‘प्रकृति’ के स्वरूप को विस्तार से समझेंगे।
प्रकृति का अर्थ
प्रकृति को गीता में भगवान की माया कहा गया है, जो सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार का कार्य करती है। यह त्रिगुणात्मक है – सत्व, रज और तम।
- सत्व: ज्ञान, शांति और संतुलन।
- रज: क्रिया, कामना और अस्थिरता।
- तम: अज्ञान, आलस्य और निष्क्रियता।
भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी अधीन है, लेकिन सजीव प्रतीत होती है क्योंकि इसमें मेरा तेज है।
“मम माया दैवी हि एषा गुणमयी।”
– गीता अध्याय 7
अप्रकट (अव्यक्त) का अर्थ
अप्रकट वह तत्व है जो इंद्रियों से परे है, जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु वह अस्तित्व में है। यह परमात्मा का वह स्वरूप है जो सभी सृष्टि में व्याप्त है, परंतु रूप, रंग, नाम आदि से रहित है।
अप्रकट, नित्य, अविनाशी और अजन्मा है। गीता में भगवान इसे अपना “उच्चतर स्वरूप” बताते हैं।
“अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तं अहुः परमां गतिम्।”
प्रकृति और अप्रकट का संबंध
- प्रकृति सृष्टि का कारण है, और अप्रकट सृष्टि का आधार है।
- प्रकृति को चलाने वाली शक्ति अप्रकट है – जो स्वयं भगवान हैं।
- जब जीवात्मा प्रकृति में आसक्त होता है, तो वह बंधन में फंसता है। जब वह अप्रकट (परमात्मा) में लीन होता है, तो मोक्ष प्राप्त करता है।
गीता में इसका महत्व
भगवान श्रीकृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त अप्रकट ब्रह्म को समझ लेता है और उसमें लीन हो जाता है, वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
आधुनिक संदर्भ में
आज के भौतिकवादी युग में जहाँ केवल दृश्य संसार को सत्य माना जाता है, गीता हमें बताती है कि दृश्य (प्रकृति) के परे भी एक अदृश्य (अप्रकट) सत्ता है, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
निष्कर्ष
प्रकृति हमें संसार से जोड़ती है, और अप्रकट हमें ईश्वर से। गीता में इन दोनों के बीच का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठकर अप्रकट परम तत्व को जान लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाता है।